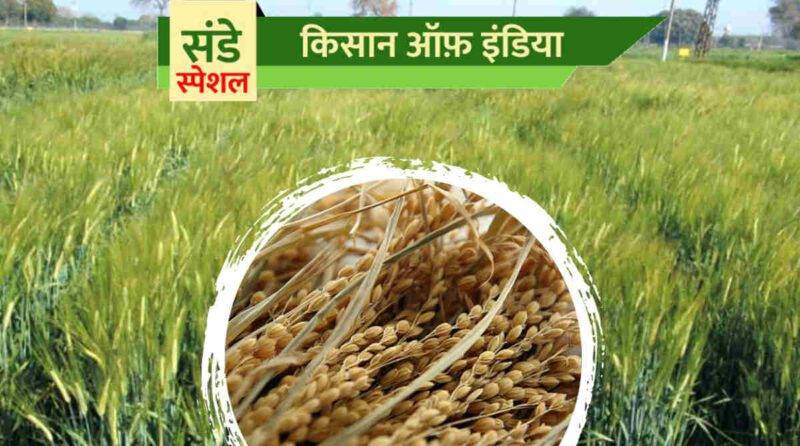जौ की खेती सारी दुनिया में होती है। विश्व में चावल, गेहूँ और मक्का के बाद जौ की पैदावार का स्थान है। वैश्विक खाद्यन्न उत्पादन में जौ की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत की है। भारत में भी ये रबी की प्रमुख फसल है। जौ को प्राचीनतम अनाज माना गया है। इसे अनाजों का राजा भी कहा गया। वेदों में भी जौ का उल्लेख है। ज़ाहिर है, भारत में जौ की खेती का इतिहास 7 हज़ार साल से ज़्यादा पुराना है। जौ एक बहुउपयोगी फसल है। इसकी पैदावार लवणीय, क्षारीय, कम बारिश वाले और बारानी इलाकों में भी हो सकती है।
देश में जौ की माँग सालाना 10 फ़ीसदी की शानदार रफ़्तार से बढ़ रही है। ज़ाहिर है कि जौ की उन्नत खेती करके किसान बढ़िया कमाई हासिल कर सकते हैं। सरकार की ओर से जौ की पैदावार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वाला क़ानूनी संरक्षण हासिल है। जौ का इस्तेमाल अनाज और पशु आहार के अलावा व्यावसायिक रूप से भी होता है। इसका औषधीय उपयोग भी काफ़ी होता है। यह विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, ज़िंक, कॉपर, प्रोटीन, रेशे तथा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इन्हीं स्वास्थ्यवर्धक गुणों की वजह से जौ को सम्पूर्ण भोजन कहा गया है।

जौ के नियमित सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है और दिल का दौरा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। मूत्र सम्बन्धी विकारों, गुर्दे की पथरी आदि में जौ का सेवन तथा इससे बनी हुई दवाइयों का प्रयोग काफ़ी प्रभावी पाया गया है। जौ में पाया जाने वाला रेशा (बीटा ग्लूकन) मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए आजकल फूड प्रोसेसिंग तकनीक से बीटा ग्लूकन को जौ से निकालकर दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलाकर उन्हें और स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा रहा है।
शिशुओं के लिए बनने वाले डिब्बा बन्द शिशु आहार में भी जौ का बहुतायत से इस्तेमाल होता है, क्योंकि जौ जहाँ एक और बेहद ऊर्जादायक अनाज है, वहीं बेहद सुपाच्य होने की वजह से शिशुओं के लिए भी मुफ़ीद पाया गया है। वैसे पारम्परिक रूप से जौ का इस्तेमाल हमारे देश में सत्तू, चपाती, शीतल पेय तथा अन्य व्यंजनों के रूप में किया जाता है। इसके भूसे का प्रयोग पशु आहार, कार्ड बोर्ड बनाने तथा मशरूम की खेती में भी होता है। जौ का बड़े पैमाने पर उपयोग कैंडी, चॉकलेट, मिल्क सिरप वग़ैरह बनाने में भी किया जा रहा है।
जौ की 60% ख़पत ब्रुईंग उद्योग में

ICAR-भारतीय गेहूँ और जौ अनुसन्धान संस्थान, करनाल के विशेषज्ञों के अनुसार, जौ की सबसे ज़्यादा ख़पत बीयर उद्योग में होती है। देश में जौ का 60 फ़ीसदी उत्पादन ब्रुईंग इंडस्ट्री (brewing industry) में खपता है। ये उद्योग अच्छी गुणवत्ता वाले जौ को हाथों-हाथ खरीद लेते हैं और जौ की अनुबन्धित खेती (contract farming) को भी बढ़ावा देते हैं। एक ज़माना था जब भारत में जौ आधारित कृषि उत्पाद बनाने वाली बहुत कम कम्पनियाँ थीं और वो भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन देशों से जौ का आयात किया करती थीं। लेकिन नब्बे के दशक में उदारवादी लाइसेंसिंग नीतियों की वजह से कई बहुराष्ट्रीय ब्रुईंग और जौ आधारित उत्पाद बनाने वाली कम्पनियाँ भारत आयीं।
चारा और अनाज के लिए जौ की दोहरी खेती
देश में जौ की खेती मुख्यतः वर्षा आधारित या सीमित सिंचाई वाली कम उपजाऊ भूमि में होती है। लेकिन राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुष्क मैदानी इलाकों में दिसम्बर-जनवरी के बीच हरे चारे की काफ़ी कमी हो जाती है। यहाँ जौ को हरे चारे के रूप में उगाया जा सकता है। चारे के लिए जौ को बोने के 50-55 दिन बाद एक कटाई ली जा सकती है। जबकि दाने की अच्छी उपज के लिए काटी गयी फसल में सिंचाई करनी चाहिए तथा कटाई के तुरन्त बाद उर्वरक डालना चाहिए। इस प्रकार जौ की द्वि-उद्देशीय खेती की जा सकती है। ऐसे दोहरे फ़ायदे के लिए RD 2715, RD 2035 और RD 2552 किस्मों को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इससे 25-35 क्विंटल अनाज और 200-250 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर उपजाया जा सकता है।
क्यों ज़रूरी है जौ की उन्नत किस्म का चयन?
जौ की खेती करने वाले किसानों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो इसकी उन्नत किस्मों को अपनाएँ। अन्यथा, पैदावार कम मिलेगी, बाज़ार में सही दाम नहीं मिलने में दिक्कतें होगी और किसान जौ की खेती से कतराएँगे। यही वजह है कि हरित क्रान्ति के बाद से देश में जौ की खेती का रक़बा घटता चला गया। हालाँकि, अब भी देश में करीब 7 लाख हेक्टेयर पर जौ की खेती होती है। वर्ष 2019-20 के दौरान 6.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगभग 16 लाख टन जौ का उत्पादन हुआ। इसकी औसत उत्पादकता 25.7 क्लिंटल प्रति हेक्टेयर रही।
आज भी कई राज्यों में मंजुला, आजाद, जागृति (उत्तर प्रदेश), BH 75 (हरियाणा), PL 172 (पंजाब), सोनू और डोलमा (हिमाचल प्रदेश) जैसी पुरानी और कम पैदावार देने वाली किस्में उगायी जा रही हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जौ की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जौ की नयी और उन्नत किस्में अपनायी जाएँ। इसका चयन क्षेत्रीय उपयोग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए। नयी किस्मों, उत्पादन तकनीकों में विकास और गुणवत्ता में सुधार की वजह से जौ की पैदावार में ख़ासा सुधार हुआ है।
| भारत के विभिन्न इलाकों के लिए अनुमोदित जौ की उन्नत प्रजातियाँ | ||||
| क्षेत्र | किस्में | बुआई की दशा | औसत उपज (क्लिंटल/हेक्टेयर) | उपयोगिता |
| उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राजस्थान (कोटा एवं उदयपुर को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ ज़िले तथा हिमाचल प्रदेश के ऊना एवं पोंटा घाटी | DWRB 92* | सिंचित, समय से | 49.81 | माल्ट |
| DWRB 91* | सिंचित, देर से | 40.62 | माल्ट | |
| DWRB 73 | सिंचित, देर से | 38.70 | माल्ट | |
| DWRUB 64 | सिंचित, देर से | 40.50 | माल्ट | |
| DWRUB 52* | सिंचित, समय से | 45.10 | माल्ट | |
| RD 2668* | सिंचित, समय से | 42.50 | माल्ट | |
| RD 2035 | सिंचित, समय से | 42.70 | खाद्य एवं चारा | |
| RD 2508 | असिंचित, समय से | 23.10 | खाद्य | |
| RD 2552 | सिंचित, समय से | 46.10 | खाद्य एवं चारा | |
| RD 2715 | सिंचित, समय से एवं निमेटोड रोधी | 26.30 | खाद्य एवं चारा | |
| NDB 1173 | सिंचित, समय से, लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए | 35.20 | खाद्य | |
| RD 2624 | असिंचित, समय से | 24.89 | खाद्य | |
| RD 2660 | असिंचित, समय से | 24.30 | खाद्य | |
| BH 902 | सिंचित, समय से | 49.75 | खाद्य | |
| BH 393 (हरियाणा) | सिंचित, समय से | 44.60 | खाद्य | |
| PL 419 (पंजाब) | असिंचित, समय से | 29.80 | खाद्य | |
| PL 426 (पंजाब) | सिंचित, समय से | 25.00 | खाद्य | |
| RD 2592 (राजस्थान) | सिंचित, समय से | 40.10 | खाद्य | |
| RD 2052 (राजस्थान) | सिंचित, समय से एवं निमेटोड रोधी | 30.68 | खाद्य | |
| उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र: पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड | BCU 73* | सिंचित, समय से | 21.60 | माल्ट |
| K 551 | सिंचित, समय से | 37.64 | माल्ट | |
| RD 2552 | लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए | 38.37 | खाद्य और चारा | |
| NDB 1173 | लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए | 35.20 | खाद्य | |
| K 560 | असिंचित, समय से | 30.40 | खाद्य | |
| K 603 | असिंचित, समय से | 29.07 | खाद्य | |
| JB 58 (मध्य प्रदेश) | असिंचित, समय से | 31.30 | खाद्य | |
| K 508 (उत्तर प्रदेश) | सिंचित, देर से | 40.50 | खाद्य | |
| नरेन्द्र जौ 2 (उत्तर प्रदेश) | सिंचित, देर से | 32.40 | खाद्य | |
| नरेन्द्र जौ 1 (उत्तर प्रदेश) | लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए | 22.30 | खाद्य | |
| नरेन्द्र जौ 3 (उत्तर प्रदेश) | लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए | 35.00 | खाद्य | |
| मध्य क्षेत्र: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान का कोटा एवं उदयपुर क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड क्षेत्र | RD 2786 | असिंचित,समय से | 50.20 | खाद्य |
| PL 751 | असिंचित,समय से | 42.30 | खाद्य | |
| JB 58 (मध्य प्रदेश) | सिंचित, समय से | 31.30 | खाद्य | |
| RD 2715 | सिंचित, समय से | 26.30 | खाद्य एवं चारा | |
| प्रायद्वीपीय क्षेत्र: महाराष्ट्र एवं कर्नाटक का मैदानी क्षेत्र | DL88 | सिंचित, समय से | 27.60 | माल्ट |
| BCU 73* | सिंचित, समय से | 29.70 | माल्ट | |
| उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र: जम्मू कश्मीर (जम्मू और कठुआ ज़िलों को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश (ऊना और पोंटा घाटी को छोड़कर) एवं उत्तराखंड (तराई क्षेत्रों को छोड़कर) | VLB 118 | वर्षा आधारित, समय से | 30.84 | खाद्य |
| HBL 113* | वर्षा आधारित/ असिंचित, समय से | 25.52 | खाद्य | |
| HBL 276** | वर्षा आधारित, समय से, ठंड एवं रतुआ रोग अवरोधी | 23.00 | खाद्य एवं चारा | |
| BHS 380 | वर्षा आधारित/ असिंचित, समय से | 20.97 | चारा | |
| BHS 352* | वर्षा आधारित /असिंचित, समय से | 21.90 | खाद्य | |
| HBL 316 (हिमाचल प्रदेश) | वर्षा आधारित /असिंचित समय से | 25.63 | खाद्य | |
| VLB 56 (उत्तराखंड) | वर्षा आधारित /असिंचित, समय से | 25.80 | खाद्य | |
| VLB 85 | वर्षा आधारित /असिंचित, समय से | 15.60 | खाद्य | |
| लवणीय/क्षारीय मिट्टी के लिए | RD2794 | सिंचित, समय से | 29.90 | खाद्य |
| NDB 1173 | सिंचित, समय से | 35.20 | खाद्य | |
| * दो पंक्ति वाले जौ ** छिलका रहित जौ | ||||
ये भी पढ़ें- Mushroom Processing: कैसे होती है मशरूम की व्यावसायिक प्रोसेसिंग? जानिए, घर में मशरूम कैसे होगी तैयार?
जौ की अनुबन्धित खेती में है बढ़िया कमाई
अभी जौ की सालाना औद्योगिक माँग करीब 3 लाख टन है। ये सालाना 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। लेकिन देश में पैदा होने वाले जौ का करीब एक-चौथाई हिस्सा ही बीयर और माल्ट बनाने के काम आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर उत्पादन में गुणवत्ता की कमी है। इसीलिए अनेक कम्पनियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में जौ की अनुबन्धित खेती को बढ़ावा दिया है। किसानों को ये कम्पनियाँ माल्ट के लिए उपयुक्त किस्मों के बीज के अलावा जौ की खेती की उन्नत तकनीकें सुलभ करवाती हैं। बुआई से लेकर कटाई तक किसानों को सुझाव और उर्वरक, खरपतवारनाशी वग़ैरह उपलब्ध कराती हैं। बदले में पूर्व निर्धारित दाम पर जौ की कटाई बाद किसानों से उनकी उपज ख़रीद लेती हैं। इस तरह जौ की व्यावसायिक खेती में किसानों की कमाई को बढ़ाने की अपार सम्भावनाएँ मौजूद हैं।
| जौ की उन्नत और व्यावसायिक खेती के लिए क्या करें और क्या नहीं? | ||||
| क्या करें? | कब करें? | कैसे करें? | क्यों करें? | क्या न करें? |
| मिट्टी की जाँच | अक्टूबर/फसल कटाई के बाद मई, जून में। | खेत के चारों कोनों से और बीच से मिट्टी का नमूना लेकर आपस में मिला लें। इस मिश्रण से करीब 500 ग्राम मिट्टी की नज़दीकी जाँच केन्द्र में भेजें। | इससे आपको अपने खेत की उर्वरा शक्ति की जानकारी प्राप्त होगी ताकि आप आवश्यकता अनुसार ही खाद का प्रयोग करें। | खेत में यदि कहीं खाद का ढेर पड़ा हो तो वहाँ से नमूना नहीं लें। खड़ी फसल वाले खेत से भी नमूना नहीं लें। क्योंकि इससे सही जाँच रिपोर्ट नहीं मिलेगी। |
| खेत की तैयारी | अक्टूबर में खेत की अच्छी जुताई कर पाटा लगा दें ताकि बुआई के लिए पर्याप्त नमी जमीन में बनी रहे। जौ की उन्नत खेती के लिए खेत को समतल होना चाहिए। | खेत की 3-4 जुताई के लिए डिस्क हैरो, कल्टीवेटर का प्रयोग करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लेजर लैंड लेवलर से खेत को समतल करें। यदि ये सुविधा गाँव में नहीं हो तो कहीं से किराये पर लेकर इस्तेमाल करें। | हल्की जुताई से मंडूसी जैसे खरपतवार का बीज ऊपर नहीं आता और ये कम उगते हैं। समतल खेत होने से पानी की बचत होती है और पूरी फसल को एक समान पानी मिलता है। | अधिक गहरी जुताई नहीं करें। ज़ीरो टिलेज से बुआई करनी हो तो हैरो का प्रयोग नहीं करें। पथरीली और पहाड़ी भूमि में लेजर लेवलिंग मुश्किल हो सकती है। |
| बुआई का तरीका | मेंड़ पर बुआई के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। जौ की बुआई ड्रिल से करनी चाहिए। | हाथ से कटाई वाले खेतों में ज़ीरो टिलेज से बुआई आसानी से हो सकती है। अच्छी बुआई के लिए ड्रिल मशीन के पीछे चलते हुए बीज और खाद की नालियों को ध्यान से देखते रहें ये खेत में ढंग से डल जाएँ। | भारी मिट्टी वाले खेतों जहाँ ढेले ज़्यादा बनते हों वहाँ मेंड़ पर बुआई नहीं करें। ड्रिल से बुआई करने से पौधों का जमाव एक जैसा रहता है और समय की बचत होती है। छिड़काव विधि से पौधों की संख्या कहीं अधिक और कहीं कम हो जाती है तथा पक्षियों के बीज खा जाने की आशंका रहती है। | ढेले अधिक बनने की वजह से मेंड़ बनाने में परेशानी आती है
और अंकुरण भी ठीक से नहीं होता। ड्रिल से बुआई के बाद पाटा नहीं लगाएँ अन्यथा बीज ज़्यादा गहराई में दब जाते हैं। |
| उन्नत प्रजाति का चुनाव | अक्टूबर में | अपने नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ/ मित्रों से विमर्श करके अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त , उच्च गुणवत्ता और उत्पादन वाली किस्म ही चुनें। | उन्नत किस्म के इस्तेमाल से न सिर्फ़ उपज बढ़ेगी बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली की फसल का बाज़ार में दाम भी ज़्यादा मिलेगा। | जौ की पुरानी किस्मों से बचें। उसमें बीमारियों से नुकसान की आशंका होती है तथा उत्पादन भी कम मिलती है। |
| सन्तुलित उर्वरक का प्रयोग | बुआई के समय एवं पहली सिंचाई के पश्चात। आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों का प्रयोग करें। | आधी नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का इस्तेमाल बुआई के वक़्त और बाक़ी नाइट्रोजन को पहली सिंचाई के बाद छिड़काव विधि से डालना चाहिए। | सन्तुलित खाद से सभी पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध होते हैं। इससे फसल स्वस्थ रहती है और उपज अच्छी मिलती है। | एक पोषक तत्व की कमी दूसरे की उपलब्धता को प्रभावित करती है। इसीलिए खाद और बीज को एक ही गहराई पर नहीं डालें। वर्ना, अंकुरण और पैदावार प्रभावित होगी। |
| सिंचाई | अक्टूबर में बुआई से पहले सिंचाई/ पलेवा करें। इसके बाद फसल की ज़रूरत और पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई दें। | खेत के चारों ओर मेंड़ बना दें और खेत को 4-5 हिस्से बाँटकर पानी देने से सिंचाई जल्दी और समान मात्रा में हो जाती है। | खेत की तैयारी में मदद मिलेगी, अंकुरण बढ़िया होगा तथा फसल की बढ़वार अच्छी रहेगी। पानी का सदुपयोग भी होगा। | खेत में बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें अन्यथा फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। |
| खरपतवार नियंत्रण
|
बुआई के 30-35 दिन बाद। | खरपतवारनाशी के एकसमान छिड़काव के लिए इसकी उचित मात्रा को फ्लैट फैन नोजल से स्प्रे करें। | खरपतवारों से उपज कम मिलती है और आर्थिक नुकसान होता है। | जिन खरपतवारनाशियों में आपसी तालमेल नहीं हो उसे स्प्रे नहीं करें। जौ की फसल में गेहूँ के दवाएँ नुकसान कर सकती हैं। |
| रोग नियन्त्रण | अक्टूबर से मार्च
|
स्वस्थ बीज तथा रोग रोधी किस्मों के प्रयोग से बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। | सही प्रजाति का चयन और इस्तेमाल करें। | जिन किस्मों की सिफ़ारिश नहीं हो उसका इस्तेमाल नहीं करें। इससे रोग का ख़तरा हो सकता है। |
| बीजोपचार | बुआई के समय | बीजोपचार से कंडुवा और मिट्टी से जुड़ी बीमारियों भय मिट जाता है। अंकुरण अच्छा होगा तो पौधे स्वस्थ होंगे और उनकी रोगों से मुक़ाबले की क्षमता भी बढ़ेगी। | बीजोपचार के लिए बीज शोधन ड्रम का प्रयोग करें। वीटावैक्स 75 WP दवा की 50 ग्राम मात्रा से 40 किलोग्राम जौ का बीज उपचारित करें। इसके एक दिन बाद इस बीज की बुआई करें। | बीजोपचार के बग़ैर बुआई नहीं करें। |
| दीमक की रोकथाम के लिए उपचार | पहली सिंचाई के 3-4 दिन बाद। | कीट रसायन से उपचारित मिट्टी डालने से दीमक के प्रकोप से बचा जा सकता है। दीमक से बचाव के लिए क्लोरपाईरिफॉस की 4.5 मिली मात्रा से एक किलोग्राम बीज उपचारित करें। | दीमक प्रभावित इलाकों में मेंड पर गेहूँ की फसल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खड़ी फसल वाले खेतों में दीमक के उपचार के लिए प्रति हेक्टेयर 3 लीटर क्लोरपाईरिफॉस को 20 किलोग्राम बालू या बारीक मिट्टी को 2-3 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रभावित खेत में बुआई के 15 दिन बाद बिखेरें। | जहाँ दीमक का प्रकोप नहीं हो वहाँ उपचार नहीं करें। दीमक रोधी दवा के इस्तेमाल के लिए खेत में उचित नमी का होना ज़रूरी है। नमी कम होने पर बुरकाव नहीं करें। |
| चेपा (माई) | चेपा दिखाई
देने पर |
इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करने से माहू यानि चेपा को दूर रख सकते हैं। माहू अक्सर खेत के किनारों से पनपता शुरू होता है और फिर खेत में फैलता है। इसलिए किनारों पर छिड़काव करके इस कीट से बचाव करना चाहिए। | चेपा की रोकथाम के लिए इमीडाक्लोप्रिड (कान्फीडोर 200 SL) दवा को 15 मिली प्रति 35 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत के किनारों पर 2-3 मीटर तक छिड़काव करें। | चेपा से छुटकारे के लिए पूरे खेत में छिड़काव नहीं करें। इससे ‘लेडी बर्ड बीटल’ जैसे मित्र कीट भी प्रभावित होते हैं। इन मित्र कीटों का खेत में सक्रिय रहना अति आवश्यक है। |
| कटाई एवं मढ़ाई | मार्च के अन्त से लेकर अप्रैल का पहला पखवाड़ा | दाने को चबाकर देखना चाहिए यदि दाँत से काटने में आवाज़ आती है तो फसल कटाई के लिए तैयार है। यदि दाना काटने में और ज़ोर लगाना पड़े तो समझिए उपज भंडारण के लिए तैयार है। कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर तथा हाथ से कटाई के बाद थ्रेशर का प्रयोग करें। | उचित समय पर कटाई से फसल की अच्छी गुणवत्ता मिलती है। सही ढंग से भंडारण करने पर दानों में कीड़े लगने का ख़तरा कम हो जाता है और उनकी अंकुरण क्षमता बनी रहती है। | यदि दानों में नमी ज़्यादा हो तो कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई नहीं करें। इससे दाने कट जाते हैं, उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और बाज़ार में दाम कम मिलता है। |
| भंडारण | जौ के भंडारण के लिए दानों को अच्छी तरह से सुखा लें। फिर नमी रहित भंडारगृह में भंडारण करें। बरसात में कीटनाशक का प्रयोग करें। | बरसात में खुला रखने पर जौ की उपज हवा से नमी को आसानी से सोख लेती है। इससे कीड़े लगने का ख़तरा रहता है। | यदि दानों में नमी ज़्यादा है तो भंडारण करने से परहेज़ करें और फसल की सही ढंग से सुखाने से समझौता नहीं करें। | |
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।