उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब भी पारम्परिक और मिश्रित खेती (Traditional and Mixed Farming) ही ज़्यादा प्रचलित है। क्योंकि वहाँ खेती की ज़मीन काफ़ी कम है। जोतो का आकार बहुत छोटा है। ट्रैक्टर और अन्य मशीनों से खेती करने की गुंज़ाइश ख़ासी कम है। उत्तराखंड में व्यायसायिक खेती बहुत कम है।
वहाँ ज़्यादातर किसान मुख्य रूप से अपनी ख़पत के लिए ही खेती करते हैं। उनकी पैदावार ही बाज़ार में कम ही जाती है। पहाड़ी इलाकों में पारम्परिक खेती को मिश्रित खेती भी कहते हैं। इसकी एक विधि ‘बारहनाजा’ (बारह किस्मों के अनाज) हैं।
बारहनाजा में अनाज के अलावा सब्ज़ियाँ और मसालों की पैदावार भी एक साथ ही की जाती है। इससे एक ओर कृषि में विविधता बनी रहती है तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की थाली बहुरंगी व्यंजनों से सज जाती है। अलग-अलग मौसम में तरह-तरह का भोजन वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्यकर माना जाता है। बारहनाजा से जुड़ी ज़मीन और फ़सल के लिए जैविक खाद (Organic manure) ही बेहतरीन है, क्योंकि जैविक खाद और मिश्रित खेती ही प्रकृति के सबसे अनुकूल हैं। इससे जहाँ ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है वहीं फ़सलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है।

मिश्रित खेती का वर्गीकरण
पहाड़ी इलाकों में होने वाली मिश्रित खेती में जो फ़सलें एक साथ पैदा हो सकती हैं उन्हें भी मौसम के अनुसार तीन वर्गों में रखा जा सकता है। खरीफ़ और जायद (अप्रैल से अक्टूबर), रबी (नवम्बर से अप्रैल) और माध्यमिक फ़सलें (मई से अगस्त)। जायद के तहत घर के आसपास की क्यारियों में सब्ज़ियाँ उगाते हैं। मिश्रित खेती का स्वरूप इस प्रकार है –
- धान, कौनि, मादिरा, बाजरा, तिलउरद, ककड़ी, उगल, मक्का, भिंडी, मूली
- गेहूँ, मटर, सरसों, चना, मसूर
- जौ, मटर, सरसों, चना, मसूर
- मक्का, भिंडी, मूली, लोबिया
- मडुवा (रागी), बाजरा, भट्ट, उरद, लोबिया, चुवा
- मादिरा, मडुवा, भट्ट, बाजरा
मिश्रित खेती में मडुवा, चौलाई, कुट्टू, ज्वार, राजमा, उरद, मूँग, गहत, भट्ट, रेन्स, नौरंगी दाल जैसी फ़सलें एक साथ बोई जाती हैं। इसके कई फ़ायदें हैं। दलहन की फ़सलें खेत में नाइट्रोजन को सन्तुलित रखती हैं। दूसरा फ़ायदा रोगों से सम्बन्धित है, क्योंकि आम तौर पर किसी रोग का प्रकोप होने पर एक-दो फ़सलें ही उससे प्रभावित होती हैं। सूखे या ज़्यादा बारिश के बावजूद कुछ फ़सलें बच जाती हैं।
इतिहासकार पद्मश्री शेखर पाठक बताते हैं कि ‘ब्रिटिश काल के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि जब देश में अकाल पड़ता था तो पहाड़ी इलाका उतना प्रभावित नहीं होता था जितना मैदानी क्षेत्र। क्योंकि पहाड़ों में प्रतिकूल मौसम में भी कुछ न कुछ पैदावार हो ही जाती थी या जंगलों से भी कई तरह की भोजन योग्य वनस्पतियाँ या फल-मूल मिल ही जाते थे।’
शेखर पाठक की बात को आगे बढ़ाते हुए बीज बचाओ आन्दोलन के प्रणेता विजय जड़धारी कहते हैं कि ‘अगर कभी जंगली जानवरों का कहर फ़सल पर टूट पड़ता है तो जानवर भी अपनी आदत के मुताबिक कुछ फ़सलों को खाते हैं और तो कुछ को छोड़ देते हैं।’

ज़रूरी है पारम्परिक खेती को लाभकारी बनाना
पारम्परिक खेती के फ़ायदों पर ज़ोर देते हुए विजय जड़धारी कहते हैं कि ‘आज हमारे मन में यह बात डाली जा चुकी है कि ज़्यादा कीटनाशक और रासायनिक खाद के साथ हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल से ही किसान का भला होगा। उसकी तरक्की होगी। लेकिन ये सच नहीं है। किसान वहीं आत्महत्याएँ कर रहे हैं, जहाँ वो अपने लिए कम और बाज़ार के लिए उत्पादन पर अधिक ज़ोर देते हैं और एक या दो फ़सलों पर ही निर्भर रहते हैं।’
ज़ाहिर है हमें परम्परागत खेती को लाभकारी बनाने पर ध्यान देना होगा। इसका लाभकारी होना ही व्यक्ति और समष्टि, दोनों के हित में है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर आप किसी चीज़ के आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं तो आप विकास विरोधी हैं। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से ग़लत है। पहाड़ी इलाकों में परम्परगत खेती को बढ़ावा देना प्रकृति ही नहीं, किसानों के भी हित में है। क्योंकि आधुनिक खेती प्रकृति को वश में करके उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती है, जबकि परम्परागत खेती में प्रकृति से सम्बन्ध स्थापित रहता है।
आधुनिक खेती से कुछेक वर्षों के लिए उत्पादन भले ही बढ़ जाता हो, लेकिन ज़्यादा कीटनाशक और रासायनिक खाद की भारी क़ीमत ज़मीन और उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती है। इसीलिए अब बाज़ार में उस ओर्गनिक फूड की माँग तेज़ी से बढ़ रही है जो अपेक्षाकृत महँगे होते हैं। कुछ दशक पहले मडुवा, मादिरा, कौनी, बाजरा जैसे अनाज को ग़रीबों का भोजन कहा जाता था, उन्हें खाना अब बेहतर माना जाता है। अब मल्टी ग्रेन आटा को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें कई अन्य अनाज शामिल होते हैं।
दरअसल, परम्परागत अनाज अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। मडुवा (रागी) और रामदाना (चौलाई) को रक्तचाप और कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित करने के लिए मुफ़ीद माना जाता है। ओर्गनिक फल-सब्जियाँ इसलिए भी महँगी मिलती हैं, क्योंकि इसमें इनका क़ुदरती गुण सबसे अधिक पाये जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि आधुनिक हाईब्रिड बीजों की अपेक्षा परम्परागत बीजों की पैदावार भले ही कम हो, लेकिन यदि इनकी खेती जैविक खाद के साथ की जाती है तो इससे पैदा होने वाली उपज में पौष्टिक तत्वों की भरमार होती है। इसीलिए अब किसानों में पारम्परिक बीजों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
यह लेख प्रदीप पांडे ने Kisanofindia.com के लिए लिखा है।
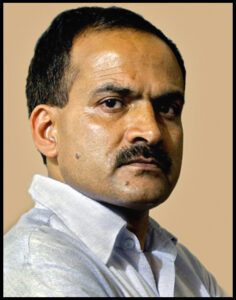 प्रदीप पांडे उत्तराखंड के बहुचर्चित फोटोग्राफर हैं। पर्वतारोहण एवं पहाड़ी क्षेत्रों की लंबी यात्राओं से उनका विशेष लगाव है। पहाड़ से जुड़े विषयों पर वो अक्सर लिखते रहे हैं। संप्रति बैंक अधिकारी के पद पर कार्यरत प्रदीप नैनीताल के निवासी हैं।
प्रदीप पांडे उत्तराखंड के बहुचर्चित फोटोग्राफर हैं। पर्वतारोहण एवं पहाड़ी क्षेत्रों की लंबी यात्राओं से उनका विशेष लगाव है। पहाड़ से जुड़े विषयों पर वो अक्सर लिखते रहे हैं। संप्रति बैंक अधिकारी के पद पर कार्यरत प्रदीप नैनीताल के निवासी हैं।


