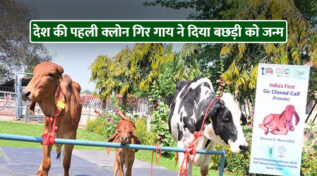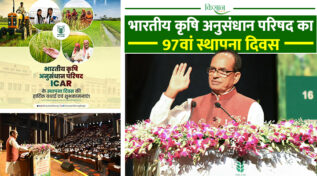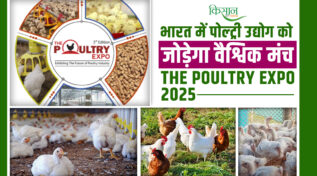किसान अच्छी तरह जानते हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से उनकी फ़सलों की पैदावार चाहे जितनी बढ़ी हो लेकिन उनके खेतों का उपजाऊपन, पैदावार की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी है। खेतों से रिसने वाले ज़हरीले रसायनों की वजह से भूजल भी बेहद प्रदूषित हुआ है और प्रदूषित आहार से मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। किसान अब ये भी बख़ूबी समझने लगे हैं कि इन सभी समस्याओं का अब सिर्फ़ एक ही उपाय है कि सदियों पुरानी जैविक खेती की ओर वापस लौट चलें क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल से वर्जित होता है।
सभी किस्म की जैविक खाद के बारे में विस्तृत और प्रमाणिक जानकारियाँ ‘किसान ऑफ़ इंडिया’ पर उपलब्ध हैं। जैसे कम्पोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट, बायोचार, हरी खाद, मटका खाद, नील हरित शैवाल, अजोला, ग्लिरिसिडिया, जीवाणु खाद, पुनर्नवा जल आदि। अब बात जैविक कीटनाशकों की। ये भी जैविक खेती का अभिन्न अंग है क्योंकि फ़सलों की बीमारियों और कीटों वग़ैरह से निपटने के लिए जैविक कीटनाशकों या ‘जैविक रोग-कीट नियंत्रण’ की भी ज़रूरत पड़ती है।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, कीटों और रोगों पर नियंत्रण का एकमात्र स्थायी समाधान यही है कि किसान विभिन्न फ़सल चक्र को अपनाएँ, ताकि कीट और फ़सलों का आपसी प्राकृतिक सामंजस्य बना रहे। हालाँकि, फ़सल चक्र को पूरी कुशलता से अपनाने के बावजूद रोग और कीट नियंत्रण की चुनौती सामने आ सकती है। इसीलिए जैविक खेती से जुड़े किसानों को भी जैविक रोग-कीट नियंत्रण की भी विस्तृत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ताकि वो इसे प्रभावी ढंग से अपना सकें।
जैविक रोग-कीट नियंत्रण की विशेषताएँ
जैविक रोग-कीट नियंत्रण भी एक तरह की चिकित्सा पद्धति ही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे मिट्टी, पानी और हवा के पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और खाद्य पदार्थों के ज़रिये मानव शरीर में पहुँच रहे ज़हरीले रसायनों से मुक्ति पाने का रास्ता भी साफ़ होता है। जन्तु जगत की तरह पादप जगत पर भी विषाणु, जीवाणु, कवक के अलावा अनेक किस्म के कीट-पतंगों और खरपतवार का हमला होता रहता है। ये हमलावर रोगजनक कहलाते हैं और इन्हें भी संक्रामक और ग़ैर संक्रामक श्रेणी में बाँटा जाता है।
जैविक रोग-कीट नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें पौधों के रोगकारकों के नियंत्रण के लिए दूसरे जीवों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक या अनेक सूक्ष्मजीवियों का उपयोग करके बीमारियों पर काबू पाया जाता है। ऐसे सूक्ष्मजीवी ही जैविक रोगनाशक कहलाते हैं। ये रोगकारकों की संख्या घटाते हैं और उनकी वृद्धि रोकते हैं। इससे जहाँ रोगों की संक्रमण क्षमता घटती है वहीं उससे छुटकारा भी मिल जाता है।
जैविक रोग-कीट नियंत्रण की प्रक्रिया और विधि
जैविक नियंत्रण एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य रोगकारकों के उन बुनियादी तत्व को निष्क्रिय बनाना है जिससे उनकी वंशवृद्धि होती है। इस काम को जैविक रोग नाशक की भूमिका निभाने वाले सूक्ष्मजीव करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है मानो फ़सल को नुकसान पहुँचाने वाले रोगकारकों के पीछे ऐसे शिकारी जीव छोड़ दिये जाएँ जो उनका सफ़ाया कर दें। इस तरह जैविक नियंत्रण का मूल मंत्र वो प्राकृतिक भोजन चक्र ही है, जिससे सम्पूर्ण प्राणी-जगत बँधा हुआ है।
जैविक नियंत्रण में कवक और जीवाणु, दोनों प्रकार के जैविक रोग नाशक सूक्ष्मजीव प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इनमें ट्राइकोडर्मा हारजीएनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, एस्परजिलस नाइजर, बेसिलस सब्टीलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस प्रमुख हैं। ये रोगकारकों की कोशिका भित्ति (nucleolus) में पाये जाने वाले उस एंजाइम को या तो नष्ट करते हैं या फिर उसकी प्रजजन अथवा वृद्धि दर को बाधित करते हैं जो रोगकारकों को जीवित (survival) रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। ट्राइकोडर्मा पाउडर का उपयोग अम्लीय मिट्टी में करना चाहिए और स्यूडोमोनस पाउडर का उपयोग ट्राइकोडर्मा पाउडर के लिए किया जाना चाहिए।
ट्राइकोडर्मा एक बेहद व्यापक प्रभाव वाला जैविक रोग नियंत्रक है। इसके जैव उत्पाद की क्षमता बहुत विस्तृत, स्थिर और सरल होती है। इसकी विकसित किस्में 10-45 डिग्री सेल्सियस तापमान और 8 प्रतिशत नमी पर स्थिर रहती हैं। इसका मानव स्वास्थ्य, मिट्टी में पाये जाने वाले लाभदायक जीवों और पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बल्कि जैविक रोग नियंत्रक के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
जैव नियंत्रकों को प्रयोग करने की विधियाँ
बीजोपचार विधि: इस विधि में 10 ग्राम पाउडर प्रति किलोग्राम बीज उपचार के लिए उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले जैव नियंत्रक के पाउडर को पानी में घोल लेते हैं। फिर बीज को इस घोल में डाल देते हैं, ताकि वो ढंग से उपचारित हो जाए। घोल में पानी की मात्रा उतनी ही रखनी चाहिए जिससे बीजोपचार के बाद घोल बचे नहीं।
चिकने बीजों जैसे मटर, अरहर, सोयाबीन आदि के उपचार के लिए घोल में गोंद, सैलूलोज जैसा कुछ चिपकने वाला पदार्थ भी मिलाना चाहिए ताकि बीज पर जैव नियंत्रक अच्छी तरह से चिपक जाएँ। इसके बाद उपचारित बीज को छायादार फर्श पर फैलाकर एक रात के लिए रख देते हैं और अगले दिन इनकी बुआई करते हैं।
छिड़काव विधि: इस विधि में प्रति लीटर पानी में 5-10 ग्राम जैव नियंत्रक पाउडर का घोल बनाकर इसका मशीन (स्प्रेयर) से छिड़काव कर सकते हैं।
पौध उपचार विधि: इस विधि में पौधशाला से उखाड़कर पौधों की जड़ को पानी में अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसे आधा घंटे के लिए जैव नियंत्रक घोल में रखते हैं और फिर खेतों में रोपाई करते हैं। इस तरह का पौध उपचार मुख्यतः धान, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च आदि फ़सलों के लिए किया जाता है।
सावधानियाँ: जैविक रोग नाशक सूक्ष्मजीवों से बीजों के उपचारित करने से पहले ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि इन्हें खेतों में डालने या बुआई से पहले मिट्टी में नमी का उचित स्तर मौजूद रहे। जैविक रोग नाशक सूक्ष्मजीव के पाउडर का छिड़काव हमेशा शाम के वक़्त ही करना चाहिए। जैव नियंत्रकों का उपयोग उनकी शेल्फ लाइफ़ या निर्माताओं की ओर से निर्धारित अवधि के दौरान ही कर लिया जाना चाहिए। वर्ना अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा।
घरेलू जैविक कीटनाशक
जैविक कीटनाशकों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि किसान इसे अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों से ख़ुद तैयार कर सकते हैं। इनसे जहाँ उनकी बाज़ार पर निर्भरता नहीं रहती, वहीं खेती की लागत भी काबू में रहती है। इसीलिए, अब बात ऐसे ही कुछ आसान और जाँचे-परखे उपायों की जिनका खेती में इस्तेमाल करके किसान सदियों से रोगों और कीटों से बचाव करते रहे हैं।
नीम की पत्तियाँ: नीम की पत्तियों से बनने वाले जैविक कीटनाशक का प्रयोग कवक जनित रोगों के अलावा सूंडी, माहूं, जैसे कीटों से बचाव और रोकथाम में अत्यन्त लाभकारी होता है। एक एकड़ ज़मीन में छिड़काव के लिए 10-12 किलोग्राम नीम की पत्तियों का प्रयोग करें। इसका 10 लीटर घोल बनाने के लिए 1 किलोग्राम पत्ती को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह पत्तियों को अच्छी तरह कूटकर या पीसकर और पतले कपड़े से छानकर वापस उसी पानी में मिलाकर घोल बना लें। फिर शाम को छिड़काव से पहले नीम के इस रस में 10 ग्राम देसी साबुन भी घोल लें।
ये भी पढ़ें – नीम का पेड़ क्यों है सर्वश्रेष्ठ जैविक कीटनाशक (Organic Pesticide), किसान ख़ुद इससे कैसे बनाएँ घरेलू दवाईयाँ?
नीम का तेल: नीम का तेल इसके बीजों से निकाला जाता है। नीम के तेल का 1 लीटर घोल बनाने के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर इसमें 1 ग्राम देसी साबुन या रीठे का घोल मिलाएँ। एक एकड़ की फसल में 1 से 3 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। इस घोल का इस्तेमाल इसे बनाने के तुरन्त बाद करें। वर्ना तेल अलग होकर सतह पर फैलने लगता है और घोल प्रभावी नहीं रह जाता। नीम के तेल के छिड़काव से गन्ने की फसल में तनाबेधक और शीर्ष बेधक कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नीम का तेल कवकजनित रोगों पर भी प्रभावी है।
नीम की खली: कवक और मिट्टीजनित रोगों के लिए एक एकड़ खेत में 40 किलोग्राम नीम की खली को पानी और गौमूत्र में मिलाकर खेत की जुताई करने से पहले डालें, ताकि यह अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाए।
बकायन (डैकण): पहाड़ों में नीम की जगह बकायन को प्रयोग में ला सकते हैं। एक एकड़ के लिए बकायन की 5 से 6 किलोग्राम पत्तियों की आवश्यकता होती है। छिड़काव पत्तियों की दोनों सतहों पर करें। नीम या बकायन पर आधारित कीटनाशकों का प्रयोग हमेशा सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों के कारण इसके तत्व नष्ट होने का खतरा होता है। इसके साथ ही शत्रु कीट भी शाम को ही निकलते हैं, जिससे इनको नष्ट किया जा सकता है। बकायन के तेल, पत्तियों, गिरी और खली के प्रयोग और छिड़काव की विधि भी नीम की तरह है।
गौमूत्र: गौमूत्र कीटनाशक के अलावा पोटाश और नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत भी है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल फल, सब्जी तथा बेल वाली फ़सलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। गौमूत्र को 5 से 10 गुना पानी के साथ मिलाकर छिड़कने से माहूं, सैनिक कीट और शत्रु कीट मर जाते हैं।
तम्बाकू और नमक: सब्जियों की फ़सल में किसी भी कीट और रोग की रोकथाम के लिए 100 ग्राम तम्बाकू और 100 ग्राम नमक को 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसको और प्रभावी बनाने के लिए 20 ग्राम साबुन का घोल तथा 20 ग्राम बुझा चूना मिलाएँ।
मिट्टी का तेल: रागी (कोदो) और झंगोरा (सांवां) की फ़सलों पर ज़मीन में लगने वाले कीटों से बचाव के लिए मिट्टी के तेल में भूसा मिलाकर बारिश से पहले या बारिश के तुरन्त बाद ज़मीन में इसका छिड़काव करें। इससे सभी कीट मर जाते हैं। धान की फ़सल में सिंचाई के स्रोत पर 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से मिट्टी का तेल डालने से भी कीट मर जाते हैं।
शरीफा तथा पपीता: शरीफा और पपीता के बीज भी एक प्रभावी जैविक कीट और रोगनाशक की भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। ये सूंडी को बढ़ने नहीं देते। इसके एक किलोग्राम बीज या तीन किलोग्राम पत्तियों और फलों के चूर्ण को 20 लीटर पानी में मिलाएँ और छानकर छिड़काव करें।
पंचगव्य: पंचगव्य बनाने के लिए गाय का 100 ग्राम घी, 1 लीटर गौमूत्र, 1 लीटर दूध तथा 1 किलोग्राम गोबर और 100 ग्राम शीरा या शहद या दही को मिलाकर मौसम के अनुसार चार दिनों से एक सप्ताह तक रखें। इसे बीच-बीच में हिलाते रहें। उसके बाद इसे छानकर 1:10 के अनुपात में पानी के साथ मिलाकर छिड़कें। इससे फ़सल को आवश्यक पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं।
दीमक की रोकथाम: गन्ने में दीमक की रोकथाम के लिए गोबर की खाद में आडू या नीम के पत्ते मिलाकर खेत में उनके लड्डू बनाकर रखें। बुआई के समय एक एकड़ खेत में 40 किलोग्राम नीम की खली डालें। नागफनी की पत्तियाँ 10 किलोग्राम, लहसुन 2 किलोग्राम, नीम के पत्ते 2 किलोग्राम को अलग-अलग पीसकर 20 लीटर पानी में उबाल लें। ठंडा होने पर उसमें 2 लीटर मिट्टी का तेल मिलाकर 2 एकड़ ज़मीन में डालें। इसे खेत में सिंचाई के समय भी डाल सकते हैं।
जैविक बाड़: खेतों में औषधीय पौधों की बाड़ लगाना भी कीटों और रोगों पर नियंत्रण में बेहद कारगर साबित होती है। धान के खेत की मेड़ के बीच-बीच में मंडुवा या गेंदा लगाने से कीट दूर भागते हैं तथा रोगों का प्रकोप भी कम होता है। खेतों की मेड़ों पर गेंदे के फूल और तुलसी के पौधों अथवा बकायन के पेड़, तेमरू, निर्गुण्डी (सिरोली, सिवाली), नीम, चिरायता और कड़वी की झाड़ियों की बाड़ लगाएँ। ये जैविक कीटनाशी के अलावा पशुओं से भी फ़सल की रक्षा करते हैं।
जैविक घोल: परम्परागत जैविक घोल बनाने के लिए बकायन और अखरोट की दो-दो किलोग्राम सूखी पत्तियाँ, चिरायता एक किलोग्राम पत्तियाँ, तेमरू और कड़बी की आधा-आधा किलोग्राम पत्तियों को 50 ग्राम देसी साबुन के साथ कूटकर पाउडर बनाएँ और इसका जैविक घोल तैयार करें। इसमें जब ख़ूब झाग आने लगे तो घोल इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। बुआई के लिए हल जोतने से पहले इस घोल के छिड़काव से मिट्टी जनित रोगों और कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। इस छिड़काव के तुरन्त बाद खेत में हल लगाना चाहिए। एक एकड़ खेत के लिए 200 लीटर जैविक घोल पर्याप्त है।
रोगी पौधे और बाली: रोगग्रस्त पौधों की बालियों को सावधानी से उखाड़कर जला देना भी जैविक नियंत्रक की भूमिका ही निभाता है। ऐसा करके फफूँदी, वायरस और बैक्टीरिया जनित रोगों को पूरे खेत में फैलने से रोका जा सकता है।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

ये भी पढ़ें:
- Cloning Technology Created History: ‘गंगा’ गाय के Ovum से पैदा हुई स्वस्थ बछड़ी, डेयरी क्षेत्र में बड़ी कामयाबीराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (National Dairy Research Institute), करनाल के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग तकनीक (Cloning Technology Created History) के जरिए एक बड़ी सफलता पाई है। देश की पहली क्लोन गिर गाय ‘गंगा’ (Country’s first cloned Gir cow ‘Ganga’) के अंडाणुओं (Ovum) से एक स्वस्थ बछड़ी का जन्म हुआ है।
- Maize Cultivation: मक्के की खेती का उन्नत तरीक़ा क्या है, जानिए प्रगतिशील किसान ब्रजेश कुमार सेप्रगतिशील किसान ब्रजेश कुमार मक्के की खेती (Maize cultivation) में उन्नत तकनीकों से उच्च उत्पादन ले रहे हैं और आलू बीज उत्पादन में भी सराहे गए हैं।
- India Is Becoming A Global Leader In Green Energy: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा में 5 साल के टारगेट को वक्त से पहले किया पूराहरित ऊर्जा (Green Energy) के क्षेत्र में भी एक ग्लोबल लीडर (Global Leader) की भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण (Climate change and pollution) की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) को अपनी प्राथमिकता बनाया है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- धान से दाल तक, खेत से बाज़ार तक: जानिए कैसे प्रगतिशील किसान चरन सिंह ने संकर धान से बदली अपनी किस्मतउत्तर प्रदेश कानपुर देहात के गांव औरंगाबाद, पोस्ट भेवान के प्रगतिशील किसान चरन सिंह ने (Progressive farmer Charan Singh changed his fortunes), जो पिछले 20 सालों से खेती कर रहे हैं और आज न सिर्फ अपने 4 एकड़ खेत से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन गए हैं।
- रासायनिक खेती छोड़ सुषमा चौहान ने अपनाई प्राकृतिक खेती, शिमला में बनाई अपनी ख़ास पहचानप्राकृतिक खेती (Natural farming) से हिमाचल की सुषमा चौहान ने फल उत्पादन में पाया शानदार सुधार और ख़र्च घटाकर मुनाफ़ा बढ़ाया।
- Beekeeping: कैसे सफल व्यवसाय बन सकता है मधुमक्खी पालन? जानिए, प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार जाट सेमधुमक्खी पालन (Beekeeping) को सफल व्यवसाय में बदलने की जानकारी दे रहे हैं डॉ. मनोज कुमार जाट, जानिए शहद उत्पादन और वैज्ञानिक तकनीकें।
- PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना है किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम,100 चुनिंदा ज़िलों में होगी शुरूप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) को मंजूरी दे दी है। ये योजना देश के 100 चुनिंदा जिलों में शुरू की जाएगी
- New Initiative Of NABARD: GRIP, CoLab और Whatsapp चैनल से ग्रामीण भारत को मिलेगी बड़ी ताकत!नाबार्ड (NABARD) ने Graduated Rural Income Generation Programme (GRIP) की शुरुआत की है, जिसका मकसद ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस: कृषि विकास की नई उपलब्धियों का उत्सवभारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस (97th Foundation Day of ICAR) नई तकनीकों, रिकॉर्ड उत्पादन और किसानों के लिए नवाचारों का जश्न है।
- CARI-Nirbheek: देसी मुर्गी पालन में क्रांति, किसानों की आय दोगुनी करने वाला आया ‘Super Chicken’!ICAR-Central Avian Research Institute (CARI), बरेली ने ‘सीएआरआई-निर्भीक’ (CARI-Nirbheek ) नाम की एक शानदार देसी मुर्गी की प्रजाति विकसित की है, जो ग्रामीण और छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
- Fake And Substandard Fertilizers : नकली और घटिया खाद के धोखे को रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, अब होगी सख्त कार्रवाईकेंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली और घटिया गुणवत्ता वाली खाद (Fake and poor quality fertilizers) की बिक्री पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
- The Poultry Expo 2025 का इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 21 से 23 अगस्त तक होने जा रहा है आयोजनThe Poultry Expo 2025 ग्रेटर नोएडा में होगा भारत का सबसे बड़ा पोल्ट्री एक्सपो, जहां इनोवेशन, नेटवर्किंग और मार्केट की अपार संभावनाएं मिलेंगी।
- World Youth Skills Day: देश के युवा आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक खेती के साथ कृषि क्रांति में भर रहे नई उड़ान15 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) के अवसर पर आइए जानते हैं कि कैसे देश के युवा आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक खेती, कृषि-उद्यमिता (Agripreneurship) और फूड प्रोसेसिंग (Food Processing सुनहरा भविष्य बना रहे हैं।
- Ornamental Fish Rearing: सजावटी मछली पालन है फायदेमंद शौक के साथ शानदार बिज़नेस भीसजावटी मछली पालन (Ornamental Fish Rearing) न सिर्फ एक अच्छा शौक है, बल्कि एक फ़ायदेमंद बिज़नेस (Fish Farming) भी बन सकता है। अगर आपको मछलियों से प्यार है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है।
- Bio Mustard farming: सरसों की जैविक खेती को अपनाकर चुनें सालों-साल ज़्यादा उपज पाने का रास्तासरसों की जैविक खेती (Bio mustard farming) से कम लागत में अधिक मुनाफ़ा संभव है। नए शोध से साबित हुआ है कि जैविक तरीक़े से उपज को साल दर साल बढ़ाया जा सकता है।
- Google’s AI Revolution: भारतीय किसानों के लिए खुशख़बरी, AMED API नया डिजिटल साथीGoogle ने भारत के कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए एक बड़ी पहल की है। इसके तहत AMED API (Agricultural Monitoring and Event Detection) और भारतीय भाषाओं व संस्कृति को समझने वाले एआई मॉडल्स (AI Models) लॉन्च किए गए हैं। यह न सिर्फ किसानों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा।
- भोपाल में रोज़गार मेला: शिवराज सिंह चौहान ने सौंपी युवाओं को नियुक्ति पत्र, बोले – विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदमभोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने रोज़गार मेला में 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे।
- CM योगी का ‘Green Gold’ विजन: Carbon Credits से उत्तर प्रदेश बनेगा अमीर,अयोध्या बनेगा ‘ग्रीन सिटी’योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को देश का पहला ‘कार्बन क्रेडिट हब’ (Carbon Credits Hub) बनाने की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है।
- बिहार का ‘मखाना’ अब Global Star: सुपरफूड मखाना बिहार के किसानों की आय में लगाएगा पंख, जानें कैसे HS कोड ने बदला गेममखाना और इससे बने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अलग-अलग HS Code (Harmonized System Code) मिल गया है। ये निर्णय बिहार के किसानों, उद्यमियों और निर्यातकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
- गन्ने की प्राकृतिक खेती के साथ ही प्रोसेसिंग से अच्छी कमाई कर रहे हैं प्रगतिशील किसान योगश कुमार, जानिए उनका सक्सेस मंत्रगन्ने की प्राकृतिक खेती के साथ ही प्रोसेसिंग कर इनोवेटिव किसान योगेश कुमार बना रहे हैं नए उत्पाद और कमा रहे हैं बेहतर मुनाफ़ा।